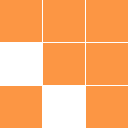 Loading...
Loading...
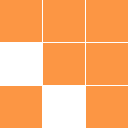 Loading...
Loading...

Overview: टेक्नोलॉजी के इस दौर में कई स्टार्टअप और कंपनियां कृषि सुधार के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजी किसानों को फसल सुरक्षा से लेकर उत्पाद की बिक्री तक मदद करती हैं। हालांकि, कई बार इन समाधानों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते क्योंकि किसान इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते। जब किसान और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ मिलकर काम करेंगे, तब समाधान अधिक उपयोगी और प्रभावी होंगे।
मैंने यहां जो कुछ लिखा है, वह इस विषय की केवल एक शुरुआत है। इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और मैं भी बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ। मुझसे पूछा जाए तो कहूंगी कि आज का यह विषय गंभीर है और टेक्निकल भी, पर मैंने यहां इसे सरल शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। किसान और टेक्नोलॉजी, इस विषय पर लिखने के लिए मैंने ना कोई बड़ी रिसर्च और ना ही कोई अध्ययन किया है, बल्कि किसानों के साथ और उनके लिए काम करते हुए जो कुछ भी मैंने सीखा और अनुभव किया उसी को यहां शब्दों में ढाला है। मैं आपसे इस विषय में जो कुछ भी साझा करना चाहती हूँ यह लेख उस श्रृंखला की पहली कड़ी है|
टेक्नोलोजी के इस समय में कई स्टार्टअप और जानी मानी कंपनियां कृषि में सुधार के लिए नई-नई टेक्नोलॉजी/एप्लिकेशन विकसित कर रही हैं। यह सुधार के उपाय किसानों को फसल सुरक्षा से लेकर उत्पाद की बिक्री तक की प्रक्रिया में अलग-अलग तरीकों से सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए वे किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझते हैं और फिर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं। हालांकि, कई बार इन समाधानों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते क्योंकि टेक्नोलोजी के निर्माण की इस प्रक्रिया में किसान सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते। जब कृषि अनुभव रखने वाले किसान और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ साथ मिलकर काम करेंगे, तब जो समाधानित-टेक्नोलॉजी तैयार होगी वह हर दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी और प्रभावी होगी।
स्टार्टअप, छात्र, या बडी कंपनियां किसी भी नए विचार को उत्पाद में बदलने में विशेषज्ञों की एक टीम के साथ कई महीने लगा देते हैं। कई महीनो की मेहनत से बनी टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुँचाने के लिए एक दिन की ट्रेनिंग, सेमिनार या वर्कशॉप जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में किसानों को नई तकनीक के फायदे, इसके काम करने के तरीके और इसे कहाँ से खरीदना है जैसी अनेक जानकारियां दी जाती हैं। कई किसान तकनीकी रूप से काफी सक्षम होते हैं और उनकी बुद्धिमता भी अच्छी होती है, ऐसे किसान नई टेक्नोलॉजी को जल्दी समझ जाते हैं। यह किसान कई बार कृषि में उनके सामने आने वाली समस्या के समाधान के रूप में साधन या टेक्नोलॉजी खुद ही बना लेते हैं जो काफी हद तक बेहतर भी होती है और जिसे दूसरे किसान आसानी से अपना भी सकते हैं। हालांकि ऐसी तकनीक विकसित करने वाले किसानों के ऊपर उनके आस-पास वाले लोग हंसते हैं और उन्हें उल्टी खोपड़ी का भी कहते है पर कई बार ऐसे ही किसानों द्वारा बनी टेक्नोलॉजी देश-विदेश तक पहुंच जाती है। यह किसान नई टेक्नोलॉजी को जल्दी समझ जाते है और अपना भी लेते है, लेकिन कई किसान ऐसे भी होते है जिन्हे टेक्नोलॉजी का ज्ञान कम होता है और वे ज्यादा शिक्षित भी नही होते पर इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी बुद्धिमता या क्षमता कम होती है. वह अपने विषय में निष्णात होते हैं और उनके पास सूझबूझ और अनुभव का भंडार होता है पर नई टेक्निकल चीजें समझने में उन्हें समय लगता है इसलिए अगर उन्हें जरूरी समय और ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाए तो वह काफी अच्छे से टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं और सहजता से उपयोग में भी ला सकते हैं। अब देखिये यहाँ टेक्नोलॉजी भी है और किसान को उसकी जरूरत भी है, लेकिन केवल जरूरी ज्ञान और समय की कमी दोनों के बीच की कड़ी को कमजोर कर देती है।
अधिकांश किसान पूरी तरह से कृषि पर निर्भर होते हैं और इसी से उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। कई स्थानों पर सिंचाई की व्यवस्था होती है और कई स्थान पर नहीं भी होती, इसलिए जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां कृषि बारिश पर निर्भर रहती है या कुछ किसान खुद बोरवेल का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर पाते। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाएँ भी कृषि पर असर डालती हैं, जिससे किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब उन्हें कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताकर उसे प्रयोग में लाने को कहता है, तो उनके मन में इसके परिणामों को लेकर कई संशय उठते हैं। एक भी फसल का नुकसान होना उनके लिए आर्थिक और मानसिक रूप से भारी पड़ सकता है। फसल के नुकसान से उबर कर नई फसल की तैयारी में जुट जाना और उसके लिए धन की व्यवस्था के लिए कई बार किसान के ऊपर कर्ज भी हो जाता है । नई फसल के तैयार होने तक अपने और साथ में जुड़े सभी परिवार का भरणपोषण करना बड़ा ही हिम्मत वाला काम है। अब ऐसी परिस्थिति में किसान का पहले दूसरों के अनुभव देखकर ही नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार होना स्वाभाविक हैं। जब हम 500 - 1000 रुपये कीमत का कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसके रिव्यू देखते हैं, फिर यह तो किसानों के लिए उनके जीवन और आजीविका का सवाल है, इसलिए जब तक किसी टेक्नोलॉजी का परिणाम वह स्वयं नहीं देख लेते, अपनाने से कतराते हैं। अब इस समस्या का समाधान भी कहीं न कहीं किसी के पास अवश्य है, बस हमें इसे खोजकर किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है।
किसी भी नए व्यवसाय की शुरुआत से पहले व्यक्ति या कंपनी अपने उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और उनसे जुड़े हर पहलू पर रिसर्च करते हैं, ताकि वे एक ऐसा उत्पाद बना सकें जो उपयोग में आसान, टिकाऊ और बजट के अनुकूल हो। कृषि उपयोगी नई टेक्नोलॉजी बनाते समय भी ऐसे ही अध्ययन की आवश्यकता होती है। हालांकि किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, लेकिन यह अध्ययन सीमित संख्या के किसानों तक ही रहता है। कृषि पर भूमि, जल, जलवायु, भौगोलिक विस्तार, परिवहन, बाजार और किसानों की आर्थिक स्थिति जैसे कई कारक प्रभाव डालते हैं। हर क्षेत्र की कृषि एक समान नहीं होती, इसलिए यह जरूरी है कि कंपनियां विविध क्षेत्रों के पर्याप्त संख्या के किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को गहराई से समझें। इस को केवल कुछ घंटे की चर्चा तक सीमित न रखा जाए बल्कि रिसर्च कर्ता किसानों के साथ कुछ दिन बिताएं और कृषि से जुड़े हर पहलू को अच्छे से समझें ताकि एक बेहतर टेक्नोलॉजी का निर्माण हो सके। लेकिन अक्सर इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण हिस्से छूट जाते हैं और उत्पादित टेक्नोलॉजी कुछ क्षेत्र और कुछ किसानों तक ही सीमित रह जाती है, जिससे बाकी क्षेत्र के किसान को इसका लाभ नहीं मिलता और कंपनी को भी पर्याप्त उपयोगकर्ता भी नही मिलते। इस तरह उनके बीच की एक ओर कड़ी कम हो जाती है।
उपरोक्त बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देखना जरूरी है, जिसके बाद किसी फसल के लिए किसान की मेहनत, खर्च, और समय के महत्व की समझ बनेगी। किसान की मेहनत को समझने के लिए फसल की पूरी प्रक्रिया और लागत का विवरण मैं यहां रख रही हूं, जो मुझे गुजरात राज्य के भावनगर जिले के मीठी विरडी क्षेत्र के किसान श्री निलेशभाई गोबर भाई दिहोरा ने अपने अनुभव से बताया है। जब वह 2 बीघा खेत में बाजरे की फसल लगाते हैं, तो सबसे पहले वह जमीन की जुताई करते हैं, जिसके बाद अच्छी गुणवत्ता वाले बीज लाकर बुआई करते है। बुआई के बाद, वह समय-समय पर प्राकृतिक खाद खुद बनाते हैं और डालते हैं और खरपतवार भी हाथ से ही निकालते हैं। वह केवल प्राकृतिक खेती ही करते है इसलिए खरपतवार या फसल संरक्षण या उसकी वृद्धि के लिए किसी भी रासायनिक दवा या कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते। 90 दिनों की कडी मेहनत के बाद फसल तैयार हो जाती है, तो उसकी कटाई, सफाई और ग्रेडींग की जाती है और फसल को अच्छे से बाजार तक पहुंचाया जाता है। 2 बीघे में बाजरे की फसल की लागत लगभग 14 से 15 हजार रुपये आती है और करीब 4 क्विंटल का उत्पादन होता है. जो यह खर्च बताया है उसमें केवल खेती में लगने वाले साधनों, पदार्थों का खर्च शामिल है और कहीं भी किसान या उसके परिवार की मेहनत को गिनती में नहीं लिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, किसान फसल की देखभाल अपने बच्चे की तरह करता है। किसान का पूरा परिवार खेती के कार्य में जूटा रहता है।
बाजरे के उत्पादन की यह गणना हर किसान के लिए एक सी नही होती। अलग-अलग क्षेत्र की जमीन, हवा और बाकी में भिन्नता के अनुसार यह लागत भिन्न हो सकती है। अब ऐसे में किसी किसान को अपनी खेती में कोई नई तकनीक अपनाने के लिए कहा जाए, तो वह सबसे पहले यह सोचेगा कि, इस तकनीक के कारण फसल खराब हो गई या अच्छी नहीं हुई तो एक फसल की लागत, 3 महीने की मेहनत, दूसरी फसल के लिए पूंजी का प्रबंध और इस बीच परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। यही कारण है कि किसान नई तकनीक को तब तक नहीं अपनाता जब तक वह स्वयं दूसरे किसानों के खेत में उसके परिणाम न देख ले।
ये कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं जो टेक्नोलॉजी और किसानों को एक-दूसरे से जोड़ सकती हैं। अपने अगले ब्लॉग में, मैं इस विषय पर और लिखना चाहूंगी। इस विषय पर यदि आपका कोई सुझाव या विचार है तो जरूर बताएँ, मैं उसे भी शामिल करने की कोशिश करुंगी। इसके साथ ही में 'WeTheYuva' टीम से निवेदन करुंगी कि इस विषय के ऊपर कोई सेमिनार आयोजित करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जो कंपनी इस क्षेत्र में कार्यरत है उनके साथ जुड़ने की ओर कदम बढ़ाएं। साथ ही अपने विचार लिखें कि इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या संभावित कदम लिए जाने चाहिए?
मैंने अपनी सोच और किसानों के साथ के मेरे अनुभव के आधार पर, उपरोक्त विचार रखे हैं और मैं आगे के ब्लॉग में इसके समाधान-विकास के बारे में भी बात करना चाहूंगी । पर पाठकों से अनुरोध है कि इस विषय में आप अपने विचार भी बताएं। क्योंकि, यह सिर्फ किसानों और टेक्नोलॉजी विकसित करने वाली कंपनियों से जुड़ा प्रश्न नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन से भी इसका गहरा संबंध है।
इसी लेखका अगला भाग पढ़ने के लिये नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करे। https://wetheyuva.com/agriculture-and-technology-important-links-of-development-and-modern-life-2
Load More Comment
You may also like:


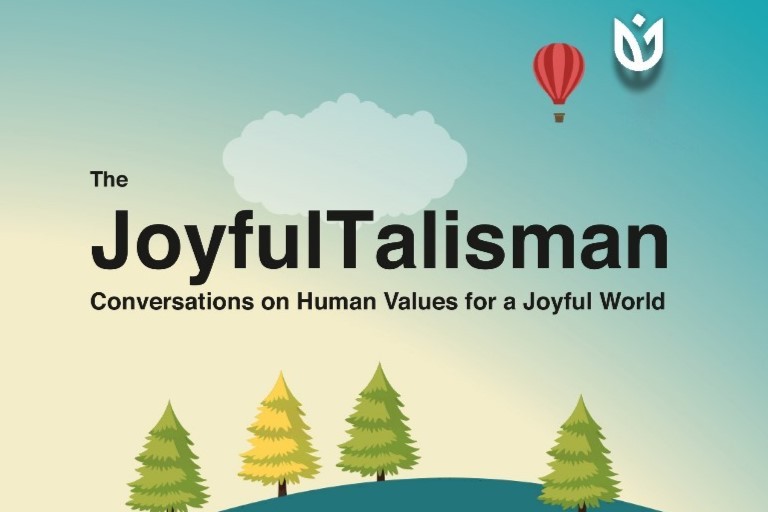

Subscribe:
Disclaimer: